समान नागरिक संहिता क्या है? संविधान इस बारे में क्या कहता है, तर्कों की व्याख्या...
समान नागरिक संहिता हमारे संविधान की शुरुआत से ही बहस का विषय रही है। इस लेख का उद्देश्य मुद्दे का कानूनी विश्लेषण प्रदान करना है | जिस समय संविधान बनाया जा रहा था, उस समय समुदायों का उनके व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होने का 150 साल लंबा इतिहास था। यह महसूस करते हुए कि ऐसी संरचनाओं का ओवरहाल एक बार में असंभव था, संविधान निर्माताओं ने यूसीसी को एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य के रूप में छोड़ दिया
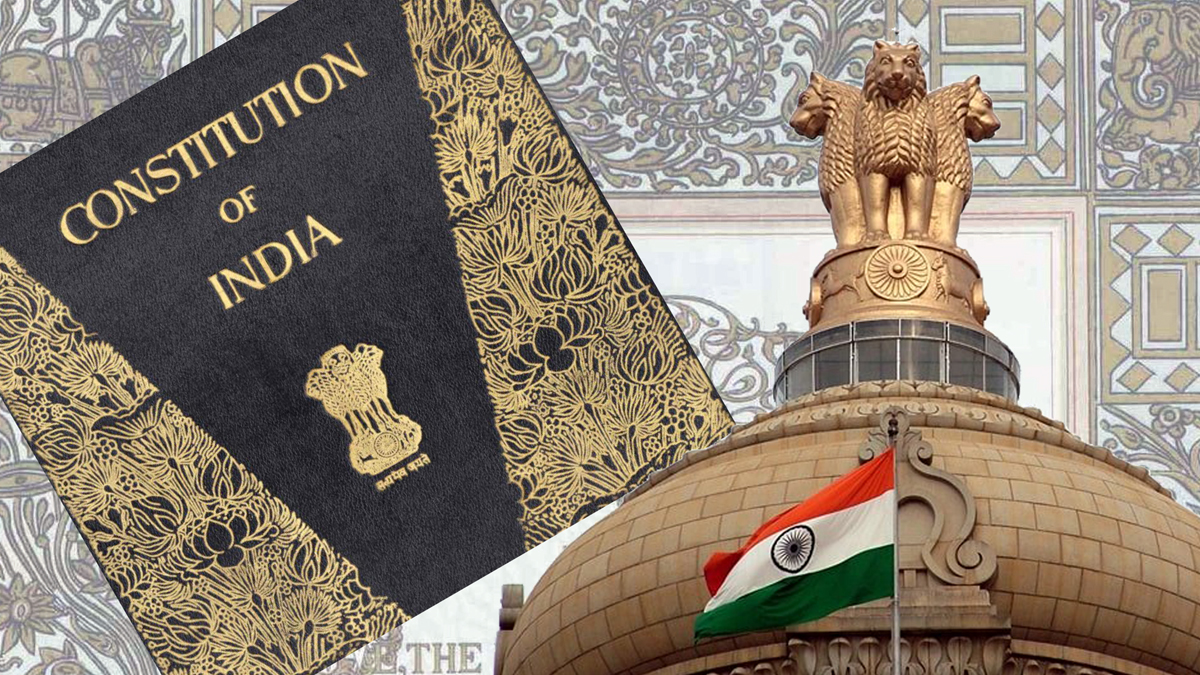
- भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की अवधारणा
- समान नागरिक संहिता के बारे में भारतीय संविधान क्या कहता है?
- भारत में विभिन्न नागरिक संहिताओं के उदाहरण:
- यूसीसी भारत में एक विवादास्पद विषय क्यों है?
- भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 44
- यूसीसीआई के समर्थन में तर्क:
- यूसीसी के विरुद्ध तर्क:
भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की अवधारणा भारत में कई दशकों से गहन बहस और चर्चा का विषय रही है।
यूसीसी के पीछे का विचार यह है कि सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनकी धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो, विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक सामान्य सेट होना चाहिए। भारत, कई धर्मों और धार्मिक कानूनों वाला एक विविध देश होने के नाते, वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून हैं।
समान नागरिक संहिता के बारे में भारतीय संविधान क्या कहता है?
भारत का संविधान, अनुच्छेद 44 के तहत, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में से एक, कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। हालाँकि, संविधान निर्माताओं ने मुद्दे की संवेदनशीलता और जटिलता को पहचानते हुए यूसीसी को लागू करना सरकार के विवेक पर छोड़ दिया। वर्षों से, विभिन्न सरकारों ने यूसीसी के कार्यान्वयन पर चर्चा और बहस की है, लेकिन यह एक विवादास्पद और राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय बना हुआ है।
भारत में विभिन्न नागरिक संहिताओं के उदाहरण:
भारत में, विवाह, तलाक, विरासत और ऐसे अन्य मामलों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानून धार्मिक ग्रंथों और रीति-रिवाजों पर आधारित हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख सहित प्रमुख धार्मिक समुदायों के अपने अलग व्यक्तिगत कानून हैं।
- हिंदू पर्सनल लॉ: हिंदू पर्सनल लॉ प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और रीति-रिवाजों से लिए गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 हिंदुओं के बीच विवाह और तलाक को नियंत्रित करता है, जबकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 विरासत से संबंधित है। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, (जो हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के अधिकारों को नियंत्रित करता है) हिंदू महिलाओं को अपने माता-पिता से संपत्ति प्राप्त करने का समान अधिकार है और हिंदू पुरुषों के समान ही अधिकार है।
- मुस्लिम पर्सनल लॉ: भारत में मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन करते हैं, जो शरिया पर आधारित है। मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 मुसलमानों के बीच विवाह, तलाक, विरासत और रखरखाव से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है।
- ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों के लिए: 1925 का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। ईसाई महिलाओं को बच्चों या अन्य रिश्तेदारों की उपस्थिति के आधार पर पूर्व निर्धारित हिस्सा मिलता है। पारसी विधवाओं को उनके बच्चों के समान हिस्सा मिलता है, यदि मृतक के माता-पिता जीवित हैं तो बच्चे का आधा हिस्सा उनके माता-पिता को दिया जाता है।
यूसीसी भारत में एक विवादास्पद विषय क्यों है?
भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर बहस बहुआयामी है और अक्सर ध्रुवीकृत होती है। यहां यूसीसी के समर्थकों और विरोधियों द्वारा प्रस्तुत कुछ प्रमुख तर्क दिए गए हैं:
धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता: भारत एक ऐसा देश है जो अपनी समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। यह कई धर्मों का घर है, प्रत्येक के अपने रीति-रिवाज, परंपराएं और व्यक्तिगत कानून हैं। आलोचकों का कहना है कि यूसीसी इस विविधता के लिए एक चुनौती है क्योंकि यह सभी नागरिकों के लिए लागू एक समान कोड के साथ व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों को बदलना चाहता है। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह का कदम देश के सांस्कृतिक ताने-बाने को कमजोर कर सकता है और धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात कर सकता है।
अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा: यूसीसी के विरोधियों द्वारा उठाई गई मुख्य चिंताओं में से एक अल्पसंख्यक समुदायों पर संभावित प्रभाव है। व्यक्तिगत कानून इन समुदायों की धार्मिक पहचान और प्रथाओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। उनका तर्क है कि समान नागरिक संहिता लागू करने से अल्पसंख्यक समूहों को प्राप्त अद्वितीय अधिकार और सुरक्षा कमजोर हो सकती है और उनकी सांस्कृतिक स्वायत्तता नष्ट हो सकती है। भारत जैसे बहुलवादी समाज में अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा और उनकी विशिष्ट प्रथाओं को संरक्षित करना महत्वपूर्ण माना जाता है।
राजनीतिक विचार: यूसीसी अक्सर राजनीतिक चालबाज़ी और दिखावे का विषय बन गया है। राजनीतिक दलों और नेताओं ने इस मुद्दे का इस्तेमाल अपने वोट बैंक को मजबूत करने या अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अपील करने के लिए किया है। धार्मिक पहचान की संवेदनशील प्रकृति और अल्पसंख्यक समुदायों पर संभावित प्रभाव ने इसे एक ध्रुवीकरण का विषय बना दिया है, जिसमें यूसीसी की खूबियों और कमियों पर वास्तविक चर्चा पर अक्सर राजनीतिक गणनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकार: यूसीसी के समर्थकों का तर्क है कि एक समान संहिता लागू करने से कुछ धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों में मौजूद भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करके लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। उनका मानना है कि एक समान संहिता विवाह, तलाक, विरासत और भरण-पोषण जैसे मामलों में समान अधिकार सुनिश्चित करेगी। हालाँकि, विरोधियों का तर्क है कि लैंगिक न्याय मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों के ढांचे के भीतर हासिल किया जा सकता है, और यूसीसी अनजाने में विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं के तहत संरक्षित महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।
राष्ट्रीय एकता: कई लोगों का मानना है कि समान नागरिक संहिता विविध धार्मिक समुदायों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देकर और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को मजबूत करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगी। जबकि अन्य लोगों का कहना है कि भारत में धार्मिक मान्यताओं और रीति-रिवाजों की विविधता को देखते हुए यूसीसी का मुद्दा अत्यधिक जटिल और संवेदनशील है।
भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 44
जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है, में कहा गया है कि राज्य को भारत के क्षेत्र में लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। हालाँकि, जैसा कि अनुच्छेद 37 में कहा गया है, निर्देशक सिद्धांत सरकारी नीतियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं और अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं।
यूसीसीआई के समर्थन में तर्क:
- भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का विचार था कि यूसीसी वांछनीय है, लेकिन संविधान सभा में महत्वपूर्ण विभाजन के बाद उन्होंने इसे फिलहाल स्वैच्छिक बने रहने का प्रस्ताव दिया।
-
“यह पूरी तरह से संभव है कि भविष्य की संसद शुरुआत करके एक प्रावधान कर सकती है कि संहिता केवल उन लोगों पर लागू होगी जो यह घोषणा करते हैं कि वे इसके लिए बाध्य होने के लिए तैयार हैं, ताकि प्रारंभिक चरण में इसे लागू किया जा सके। संहिता पूरी तरह से स्वैच्छिक हो सकती है […] ताकि मेरे दोस्तों ने यहां जो भय व्यक्त किया है वह पूरी तरह से निरस्त हो जाए।” अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था |
- अगले वर्षों में, विधायिका, न्यायपालिका और नागरिक समाज संगठनों के विभिन्न हस्तक्षेपों का उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन करना या एक समान नागरिक संहिता स्थापित करना है। इस प्रवचन में योगदान देने वाले उल्लेखनीय निर्णयों में मोहम्मद शामिल हैं। अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, जॉर्डन डिएंगदेह बनाम एस.एस. चोपड़ा, और सरला मुद्गल बनाम भारत संघ।
- शाह बानो मामले में, अदालत ने देखा कि अनुच्छेद 44 एक “मृत पत्र” बनकर रह गया है और कहा कि एक सामान्य नागरिक संहिता “परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाले कानूनों के प्रति असमान निष्ठाओं को हटाकर राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद मिलेगी”। इसमें कहा गया कि विधायिका को देश के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया है। “यदि संविधान का कोई अर्थ रखना है तो एक शुरुआत करनी होगी।”
- 1995 में सरला मुद्गल मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधान मंत्री से अनुच्छेद 44 की फिर से जांच करने का अनुरोध किया, जिसका लक्ष्य पूरे भारत में यूसीसी स्थापित करना था। हालांकि, अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप केस (1997) और लिली थॉमस केस (2000) में बाद के आदेश ) ने स्पष्ट किया कि अदालत ने सरला मुद्गल मामले में सरकार को यूसीसी बनाने का निर्देश नहीं दिया।
यूसीसी के विरुद्ध तर्क:
- 21वें विधि आयोग ने अगस्त 2018 में “पारिवारिक कानून में सुधार” पर एक परामर्श पत्र लाया जिसमें उसने कहा कि यूसीसी “इस स्तर पर न तो आवश्यक था और न ही वांछनीय”। हालाँकि, इसने सिफारिश की कि व्यक्तिगत कानूनों में भेदभाव और असमानता से निपटने के लिए सभी धर्मों के मौजूदा पारिवारिक कानूनों को संशोधित और संहिताबद्ध किया जाए।
- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने कहा: “सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता नहीं किया जा सकता है हमारा एकरूपता का आग्रह ही राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के लिए ख़तरे का कारण बन जाता है।”
- इस बात पर सहमति व्यक्त करते हुए कि प्रचलित व्यक्तिगत कानूनों के विभिन्न पहलू महिलाओं को वंचित करते हैं, आयोग ने हालांकि कहा कि “यह भेदभाव है, न कि अंतर जो असमानता की जड़ में निहित है।
- ” मानवाधिकारों पर निर्विवाद तर्क। ध्यान देने योग्य बात यह है कि विधि आयोग के सुझाव सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होते बल्कि आगे के निर्णयों के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करते हैं।



